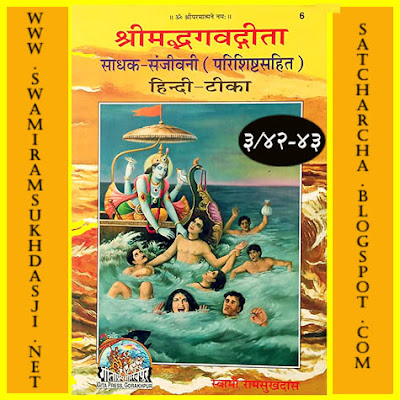Listen मार्मिक बात जब चेतन अपना सम्बन्ध जडके साथ मान लेता है,
तब उसमें संसार (भोग)-की भी इच्छा होती है और परमात्माकी भी
। जडसे सम्बन्ध माननेपर जीवसे यही भूल होती है कि वह सत्-चित्-आनन्दस्वरूप परमात्माकी
इच्छा‒अभिलाषाको संसारसे ही पूरी करनेके लिये सांसारिक पदार्थोंकी
इच्छा करने लगता है । परिणामस्वरूप उसकी ये दोनों ही इच्छाएँ (स्वरूपबोधके बिना) कभी
मिटती नहीं । संसारको जाननेके लिये संसारसे अलग होना और परमात्माको
जाननेके लिये परमात्मासे अभिन्न होना आवश्यक है;
क्योंकि वास्तवमें ‘स्वयं’ की
संसारसे भिन्नता और परमात्मासे अभिन्नता है । परन्तु संसारकी इच्छा करनेसे ‘स्वयं’ संसारसे अपनी अभिन्नता या समीपता मान लेता है,
जो कभी सम्भव नहीं; और परमात्माकी इच्छा करनेसे ‘स्वयं’ परमात्मासे अपनी भिन्नता या दूरी (विमुखता) मान लेता है,
पर इसकी सम्भावना ही नहीं । हाँ, सांसारिक
इच्छाओंको मिटानेके लिये पारमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी है । यदि पारमार्थिक
इच्छा तीव्र हो जाय तो लौकिक इच्छाएँ स्वतः मिट जाती हैं । लौकिक इच्छाएँ सर्वथा मिटनेपर
पारमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है अर्थात् नित्यप्राप्त परमात्माका अनुभव हो जाता
है१ । कारण कि वास्तवमें परमात्मा सदा-सर्वत्र विद्यमान है,
पर लौकिक इच्छाएँ रहनेसे उनका अनुभव नहीं होता । १.यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ (कठ॰ २ । ३ । १४; बृहदा॰ ४ । ४ । ७) ‘साधकके हृदयमें स्थित सम्पूर्ण कामनाएँ जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरणधर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और यहीं (मनुष्यशरीरमें ही) ब्रह्मका भलीभाँति
अनुभव कर लेता है ।’ विमुञ्चति
यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् । तर्ह्येव पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्पते ॥ (श्रीमद्भा॰ ७ । १० । ९) ‘कमलनयन ! जिस समय मनुष्य अपने मनमें रहनेवाली समस्त कामनाओंका परित्याग कर देता
है, उसी समय वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त कर लेता है ।’ ‘जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्’‒‘महाबाहो’ का अर्थ है‒बड़ी और बलवान् भुजाओंवाला अर्थात् शूरवीर । अर्जुनको
‘महाबाहो’
अर्थात् शूरवीर कहकर भगवान् यह लक्ष्य कराते हैं कि तुम इस ‘काम’-रूप शत्रुका दमन करनेमें समर्थ हो । संसारसे सम्बन्ध रखते हुए ‘काम’ का नाश करना बहुत कठिन है । यह ‘काम’ बड़ों-बड़ोंके भी विवेकको ढककर उन्हें कर्तव्यसे च्युत कर देता
है, जिससे उनका पतन हो जाता है । इसलिये भगवान्ने इसे दुर्जय शत्रु कहा है । ‘काम’ को
दुर्जय शत्रु कहनेका तात्पर्य इससे अधिक सावधान रहनेमें है, इसे
दुर्जय समझकर निराश होनेमें नहीं । प्रत्येक कामनाकी उत्पत्ति, पूर्ति, अपूर्ति और निवृत्ति होती है, इसलिये मात्र कामनाएँ उत्पन्न और नष्ट होनेवाली हैं । परन्तु
‘स्वयं’ निरन्तर रहता है और कामनाओंके उत्पन्न तथा नष्ट होनेको जानता
है । अतः कामनाओंसे वह सुगमतापूर्वक सम्बन्ध-विच्छेद कर सकता है;
क्योंकि वास्तवमें सम्बन्ध है ही नहीं । इसलिये साधकको कामनाओंसे
कभी घबराना नहीं चाहिये । यदि साधकका अपने कल्याणका पक्का उद्देश्य है२
तो वह ‘काम’ को सुगमतापूर्वक मार सकता है । २.उद्देश्य या लक्ष्य सदैव
अविनाशी (चेतन-तत्त्व‒परमात्मा)-का ही होता है, नाशवान् (संसार)-का नहीं । नाशवान्की
कामनाएँ ही होती हैं,
उद्देश्य नहीं होता ।
उद्देश्य वह होता है, जिसे मनुष्य निरन्तर चाहता है । चाहे शरीरके टुकडे-टुकड़े ही
क्यों न कर दिये जायँ,
तो भी वह उद्देश्यको
ही चाहता है । उद्देश्यकी सिद्धि अवश्य होती है, पर
कामनाओंकी सिद्धि नहीं होती, प्रत्युत नाश होता है । उद्देश्य सदा एक ही रहता
है, पर
कामनाएँ बदलती रहती हैं । कामनाओंके त्यागमें अथवा परमात्माके प्राप्तिमें
सब स्वतन्त्र, अधिकारी, योग्य और समर्थ हैं । परन्तु कामनाओंकी पूर्तिमें
कोई भी स्वतन्त्र, अधिकारी, योग्य और समर्थ नहीं है । कारण कि कामना पूरी होनेवाली
है ही नहीं । परमात्माने मानव-शरीर
अपनी प्राप्तिके लिये ही दिया है । अतः कामनाका त्याग करना कठिन नहीं है । सांसारिक
भोग-पदार्थोंको महत्त्व देनेके कारण ही कामनाका त्याग कठिन मालूम देता है । सुख (अनुकूलता)-की कामनाको मिटानेके लिये ही भगवान्
समय-समयपर दुःख (प्रतिकूलता) भेजते हैं कि सुखकी कामना मत करो; कामना
करोगे तो दुःख पाना ही पड़ेगा । सांसारिक पदार्थोंकी कामनावाला मनुष्य दुःखसे कभी बच
ही नहीं सकता‒यह नियम है; क्योंकि संयोगजन्य भोग ही दुःखके हेतु हैं (गीता‒पाँचवें
अध्यायका बाईसवाँ श्लोक) । ‘स्वयं’ (स्वरूप) में अनन्त बल है । उसकी सत्ता और बलको पाकर ही बुद्धि,
मन और इन्द्रियाँ सत्तावान् एवं बलवान् होते हैं । परन्तु जडसे
सम्बन्ध जोड़नेके कारण वह अपने बलको भूल रहा है और अपनेको बुद्धि,
मन और इन्द्रियोंके अधीन मान रहा है । अतएव
‘काम’-रूप शत्रुको मारनेके लिये अपने-आपको जानना और अपने बलको पहचानना
बड़ा आवश्यक है । ‘काम’ जडके
सम्बन्धसे और जडमें ही होता है । तादात्म्य होनेसे वह स्वयंमें प्रतीत होता है । जडका
सम्बन्ध न रहे तो ‘काम’
है ही नहीं । इसलिये यहाँ ‘काम’ को मारनेका तात्पर्य वस्तुतः ‘काम’ का सर्वथा अभाव बतानेमें ही है । इसके विपरीत यदि ‘काम’
अर्थात् कामनाकी सत्ताको मानकर उसे मिटानेकी चेष्टा
करें तो कामनाका मिटना कठिन है । कारण कि वास्तवमें कामनाकी स्वतन्त्र सत्ता है ही नहीं । कामना उत्पन्न होती
है और उत्पन्न होनेवाली वस्तु नष्ट होगी ही‒यह नियम है । नयी कामना न करें तो पहलेकी
कामनाएँ अपने-आप नष्ट हो जायँगी । इसलिये कामनाको मिटानेका
तात्पर्य है‒नयी कामना न करना । शरीरादि सांसारिक पदार्थोंको ‘मैं’, ‘मेरा’ और ‘मेरे लिये’ माननेसे ही अपने-आपमें कमीका अनुभव होता है, पर मनुष्य भूलसे उस कमीकी पूर्ति भी सांसारिक पदार्थोंसे ही
करना चाहता है । इसलिये वह उन पदार्थोंकी कामना करता है । परन्तु वास्तवमें आजतक सांसारिक पदार्थोंसे किसीकी भी कमीकी पूर्ति हुई
नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं । कारण कि स्वयं अविनाशी
है और पदार्थ नाशवान् हैं । स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान्की कामना करनेसे लाभ तो कोई होता नहीं और हानि
कोई-सी भी बाकी रहती नहीं । इसलिये भगवान् कामनाको शत्रु बताते हुए उसे मार डालनेकी
आज्ञा देते हैं । कर्मयोगके द्वारा इस कामनाका नाश सुगमतासे हो जाता है । कारण
कि कर्मयोगका साधक संसारकी छोटी-से-छोटी अथवा बड़ी-से-बड़ी प्रत्येक क्रिया परमात्मप्राप्तिका
उद्देश्य रखकर दूसरोंके लिये ही करता है, कामनाकी पूर्तिके लिये नहीं । वह प्रत्येक क्रिया निष्कामभावसे
एवं दूसरोंके हित और सुखके लिये ही करता है, अपने लिये कभी कुछ नहीं करता । उसके पास जो समय,
समझ, सामग्री और सामर्थ्य है, वह सब अपनी नहीं है, प्रत्युत मिली हुई है और बिछुड़ जायगी । इसलिये वह उसे अपनी कभी
न मानकर निःस्वार्थभावसे (संसारकी ही मानकर) संसारकी ही सेवामें लगा देता है । उसे
पूरी-की-पूरी संसारकी सेवामें लगा देता है, अपने पास बचाकर नहीं रखता । अपना न
माननेसे ही वह पूरी-की-पूरी सेवामें लगती है,
अन्यथा नहीं । कर्मयोगी अपने लिये कुछ करता ही नहीं,
अपने लिये कुछ चाहता ही नहीं और अपना कुछ मानता ही नहीं । इसलिये
उसमें कामनाओंका नाश सुगमतापूर्वक हो जाता है । कामनाओंका सर्वथा नाश होनेपर उसके उद्देश्यकी
पूर्ति हो जाती है और वह अपने-आपमें ही अपने-आपको पाकर कृतकृत्य,
ज्ञात-ज्ञातव्य और प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाता है अर्थात्
उसके लिये कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता । परिशिष्ट भाव‒भगवान्ने इन्द्रियाँ, मन और बुद्धिका नाम तो लिया है, पर ‘अहम्’ का नाम नहीं लिया । अहम् बुद्धिसे परे है । सातवें अध्यायके
चौथे श्लोकमें भी भगवान्ने बुद्धिके बाद अहम्को लिया है‒‘भूमिरापोऽनलो
वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । अहङ्कार इतीयं मे....’
। अतः यहाँ भी ‘सः’ पदसे अहम्में रहनेवाले ‘काम’ को लेना चाहिये । जबतक स्वरूपका साक्षात्कार नहीं होता,
तबतक अहम्में काम रहता है । स्वरूपका साक्षात्कार होनेपर अहम्में
काम नहीं रहता‒‘परं दृष्ट्वा निवर्तते’ (गीता
२ । ५९) । सुख तो है स्वरूपमें,
पर कामके कारण मनुष्य जड़ताको सत्ता और महत्ता देकर उससे सुख
चाहता है । जबतक जड़ताका सम्बन्ध है, तबतक ‘काम’ है, जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ‘प्रेम’ होता है । ‘काम’ अपनेमें है‒‘रसोऽप्यस्य’ (गीता २ । ५९) । अपनेमें होनेसे ही काम हमारे लिये बाधक होता है । अगर यह अपनेमें
न हो,
दूसरे (इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि)-में हो तो हमारेको क्या बाधा लगी
?
अपनेमें काम होनेसे ही स्वयं सुखी-दुःखी होता है,
कर्ता-भोक्ता होता है । वास्तविक दृष्टिसे
देखा जाय तो काम अपनेमें माना हुआ है, अपनेमें है नहीं,
तभी यह मिटता है । अतः काम अपनेमें है, पर माना हुआ है । अहम्में रहनेवाली चीजको मनुष्य अपनेमें मान लेता है । अपनेमें
अहम् माना हुआ है और उस अहम्में काम रहता है । अतः जबतक अहम् है,
तबतक अहम्की जातिका आकर्षण अर्थात्
‘काम’
होता है और जब अहम् नहीं रहता,
तब स्वयंकी जातिका आकर्षण अर्थात्
‘प्रेम’
होता है । काममें संसारकी तरफ और प्रेममें
परमात्माकी तरफ आकर्षण होता है । सम्पूर्ण त्रिलोकी, अनन्त ब्रह्माण्ड ‘विषय’ है । विषय इन्द्रियोंके एक देशमें हैं,
इन्द्रियाँ मनके एक देशमें हैं,
मन बुद्धिके एक देशमें है, बुद्धि अहम्के एक देशमें है और अहम् चेतन (स्वरूप)-के एक देशमें
है । अतः चेतन अत्यन्त महान् है, जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण त्रिलोकी,
अनन्त ब्रह्माण्ड विद्यमान हैं । परन्तु अपरा प्रकृतिके एक अंश
अहम्के साथ अपना सम्बन्ध जोड़नेके कारण मनुष्य अपनेको अत्यन्त छोटा (एकदेशीय) देखता
है ! गीता-प्रबोधनी व्याख्या‒पृथ्वी, जल, तेज, वायु आकाश, मन, बुद्धि तथा अहम्‒ये आठ प्रकारके भेदोंवाली अपरा प्रकृति है (गीता ७ । ४) । बुद्धिसे
भी पर जो अहम् है, उस अहम्के जड़-अंशमें ‘काम’ रहता है । तात्पर्य है कि कामरूप विकार अपरा प्रकृति
(जड़)-में रहता है, परा प्रकृति (चेतन)-में नहीं । परन्तु
अहम्के साथ तादात्म्य करनेके कारण उस कामरूप विकारको चेतन (जीवात्मा) अपनेमें मान
लेता है । जबतक अहम्रूप जड़-चेतनका तादात्म्य रहता है, तबतक जड़ और चेतनके विभागका ज्ञान नहीं होता । जबतक तादात्म्य
है, तभीतक ‘काम’ है । तादात्म्य टूटनेपर उस कामका स्थान ‘प्रेम’ ले लेता है । काममें संसारकी
ओर आकर्षण होता है और प्रेममें भगवान्की ओर । രരരരരരരരരര ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ इस प्रकार ॐ, तत्, सत्‒इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक
ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्रूप श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें
‘कर्मयोग’ नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ ॥ ३ ॥ इस तीसरे अध्यायका नाम ‘कर्मयोग’ है; क्योंकि कर्मयोगका जितना विशद वर्णन तीसरे अध्यायमें है,
उतना गीताके अन्य अध्यायोंमें नहीं है । तीसरे अध्यायके पद,
अक्षर और उवाच (१) इस अध्यायमें ‘अथ तृतीयोऽध्यायः’ के तीन, ‘अर्जुन उवाच’
आदि पदोंके आठ श्लोकोंके पाँच सौ बयालीस और पुष्पिकाके तेरह
पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग पाँच सौ छाछठ है । (२) इस अध्यायमें ‘अथ तृतीयोऽध्यायः’ के सात, ‘अर्जुन उवाच’
आदि पदोंके छब्बीस, श्लोकोंके एक हजार तीन सौ छिहत्तर और पुष्पिकाके पैंतालीस अक्षर
हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार चार सौ चौवन है । इस अध्यायके सभी
श्लोक बत्तीस अक्षरोंके हैं । (३) इस अध्यायमें चार उवाच हैं‒दो
‘अर्जुन
उवाच’ और दो ‘श्रीभगवानुवाच’
। तीसरे अध्यायमें प्रयुक्त छ्न्द
इस अध्यायके तैंतालीस श्लोकोंमेंसे‒पहले और सैंतीसवें श्लोकके
प्रथम चरणमें तथा ग्यारहवें श्लोकके तृतीय चरणमें ‘रगण’ प्रयुक्त होनेसे ‘र-विपुला’; पाँचवें श्लोकके प्रथम चरणमें ‘नगण’ प्रयुक्त होनेसे ‘न-विपुला’; उन्नीसवें, छब्बीसवें, और पैंतीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा आठवें और इक्कीसवें
श्लोकके तृतीय चरणमें ‘भगण’ प्रयुक्त होनेसे ‘भ-विपुला’; और सातवें श्लोकके प्रथम चरणमें
‘नगण’
और तृतीय चरणमें ‘रगण’ प्रयुक्त होनेसे ‘संकीर्ण-विपुला’
संज्ञावाले छन्द हैं । शेष तैंतीस श्लोक ठीक
‘पथ्यावक्त्र’ अनुष्टुप् छन्दके लक्षणोंसे
युक्त हैं । രരരരരരരരരര |
FOLLOW BY EMAIL
कीर्तन
Labels
- आहार-शुद्धि (13)
- कर्म-रहस्य (21)
- कल्याण-पथ (13)
- जीवनका कर्तव्य (2)
- जीवनोपयोगी कल्याण-मार्ग (14)
- दुर्गतिसे बचो (18)
- निर्वाणदिन (1)
- भगवन्नाम (27)
- सत्संगका प्रसाद (27)
- साधक-संजीवनी-0-नम्र निवेदन (3)
- साधक-संजीवनी-0-प्राक्कथन (4)
- साधक-संजीवनी-अध्याय-०१ (21)
- साधक-संजीवनी-अध्याय-०२ (67)
- साधक-संजीवनी-अध्याय-०३ (59)
- साधक-संजीवनी-अध्याय-०४ (49)
- साधक-संजीवनी-अध्याय-०५ (12)
Blog Archive
-
▼
2023
(313)
- November (9)
- October (31)
- September (30)
- August (31)
- July (31)
- June (30)
- May (31)
- April (30)
- March (31)
- February (28)
- January (31)
-
►
2022
(366)
- December (31)
- November (30)
- October (31)
- September (30)
- August (32)
- July (31)
- June (30)
- May (31)
- April (30)
- March (31)
- February (28)
- January (31)
-
►
2021
(364)
- December (31)
- November (30)
- October (31)
- September (30)
- August (31)
- July (31)
- June (30)
- May (31)
- April (30)
- March (31)
- February (28)
- January (30)
-
►
2020
(366)
- December (31)
- November (30)
- October (31)
- September (30)
- August (31)
- July (31)
- June (30)
- May (31)
- April (30)
- March (31)
- February (29)
- January (31)
-
►
2019
(365)
- December (31)
- November (30)
- October (31)
- September (30)
- August (31)
- July (31)
- June (30)
- May (31)
- April (30)
- March (31)
- February (28)
- January (31)
-
►
2018
(363)
- December (31)
- November (30)
- October (30)
- September (30)
- August (31)
- July (31)
- June (30)
- May (31)
- April (30)
- March (30)
- February (28)
- January (31)
-
►
2017
(333)
- December (27)
- November (28)
- October (31)
- September (30)
- August (31)
- July (33)
- June (3)
- May (29)
- April (30)
- March (31)
- February (29)
- January (31)
-
►
2016
(367)
- December (31)
- November (30)
- October (31)
- September (30)
- August (31)
- July (31)
- June (30)
- May (31)
- April (31)
- March (31)
- February (29)
- January (31)
-
►
2015
(368)
- December (31)
- November (30)
- October (32)
- September (30)
- August (31)
- July (31)
- June (32)
- May (31)
- April (30)
- March (31)
- February (28)
- January (31)
-
►
2014
(367)
- December (32)
- November (30)
- October (31)
- September (30)
- August (31)
- July (32)
- June (30)
- May (31)
- April (30)
- March (31)
- February (28)
- January (31)
-
►
2013
(369)
- December (31)
- November (31)
- October (31)
- September (30)
- August (31)
- July (33)
- June (30)
- May (31)
- April (30)
- March (31)
- February (29)
- January (31)
-
►
2012
(385)
- December (36)
- November (34)
- October (31)
- September (31)
- August (34)
- July (32)
- June (31)
- May (31)
- April (30)
- March (34)
- February (30)
- January (31)
मेरे स्वामीजी
स्वामीजीका जन्म वि.सं.१९६० (ई.स.१९०४) में राजस्थानके नागौर जिलेके छोटेसे गाँवमें हुआ था और उनकी माताजीने ४ वर्षकी अवस्थामें ही उनको सन्तोंकी शरणमें दे दिया था, आपने सदा परिव्राजक रूपमें सदा गाँव-गाँव, शहरोंमें भ्रमण करते हुए गीताजीका ज्ञान जन-जन तक पहुँचाया और साधु-समाजके लिए एक आदर्श स्थापित किया कि साधु-जीवन कैसे त्यागमय, अपरिग्रही, अनिकेत और जल-कमलवत् होना चाहिए और सदा एक-एक क्षणका सदुपयोग करके लोगोंको अपनेमें न लगाकर सदा भगवान्में लगाकर; कोई आश्रम, शिष्य न बनाकर और सदा अमानी रहकर, दूसरोकों मान देकर; द्रव्य-संग्रह, व्यक्तिपूजासे सदा कोसों दूर रहकर अपने चित्रकी कोई पूजा न करवाकर लोग भगवान्में लगें ऐसा आदर्श स्थापित कर गंगातट, स्वर्गाश्रम, हृषिकेशमें आषाढ़ कृष्ण द्वादशी वि.सं.२०६२ (दि. ३.७.२००५) ब्राह्ममुहूर्तमें भगवद्-धाम पधारें । सन्त कभी अपनेको शरीर मानते ही नहीं, शरीर सदा मृत्युमें रहता है और मैं सदा अमरत्वमें रहता हूँ‒यह उनका अनुभव होता है । वे सदा अपने कल्याणकारी प्रवचन द्वारा सदा हमारे साथ हैं । सन्तोंका जीवन उनके विचार ही होते हैं ।
हे नाथ ! मेरे नाथ !! मैं आपको भूलूँ नहीं !
−श्रद्धेय श्रीस्वामीजी महाराज