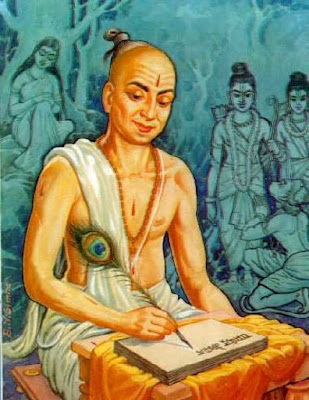(गत ब्लॉगसे आगेका)
जो आदि और
अन्तमें नहीं होता, वह मध्यमें भी नहीं होता, यह सिद्धान्त है–‘आदावन्तो च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा’ (माण्डूक्यकारिका ४/३१) । जैसे दर्पणमें मुख पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा
और वर्तमानमें प्रत्यक्ष दीखनेपर भी वह वास्तवमें है नहीं । ऐसे ही अपनेमें दोष पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा और
वर्तमानमें दीखते हुए भी वह अपनेमें नहीं है । जैसे दर्पणमें मुखकी प्रतीति है,
ऐसे ही अपनेमें दोषोंकी प्रतीति है, वास्तवमें दोष है नहीं ।
जैसे अपनेमें दोष नहीं है, ऐसे ही
दूसरेमें भी दोष नहीं हैं । सबका स्वरूप स्वतः निर्दोष
है । अतः कभी किसीको दोषी नहीं मानना चाहिये । ऐसा समझना चाहिये कि दूसरेने
आगन्तुक दोषके वशीभूत होकर क्रिया कर दी, पर न तो वह क्रिया स्थायी रहेगी तथा न
उसका फल स्थायी रहेगा । क्रिया और फल तो नहीं रहेंगे, पर स्वरूप रहेगा । अगर हम दूसरेमें दोष मानेंगे तो उसमें वे दोष आ जायँगे;
क्योंकि उसमें दोष देखनेसे हमारा त्याग, तप, बल आदि भी उस दोषको पैदा करनेमें
स्वाभाविक सहायक बन जायगा, जिससे वह व्यक्ति दोषी हो जायगा । अतः (सिद्धान्तकी दृष्टिसे)
पुत्र, शिष्य आदिको स्वरुपसे निर्दोष मानकर और उनमें दिखनेवाले दोषको आगन्तुक मानकर ही उनको (व्यवहारकी दृष्टिसे) शिक्षा देना
चाहिये । उनमें निर्दोषता मानकर ही उनके आगन्तुक दोषको दूर करनेका प्रयत्न
करना चाहिये ।
अगर मन-बुद्धिमें
कोई दोष पैदा हो जाय तो उसके वशमें नहीं होना चाहिये–‘तयोर्न
वशमागच्छेत्’ (गीता ३/३४) अर्थात् उसके अनुसार
कोई क्रिया नहीं करनी चाहिये । उसके वशीभूत होकर क्रिया करनेसे वह दोष दृढ़
हो जायगा । परन्तु उसके वशीभूत होकर क्रिया न करनेसे एक उत्साह पैदा होगा । जैसे, किसीने हमें कड़वी बात कह दी, पर हमें क्रोध नहीं
आया तो हमारे भीतर एक उत्साह, प्रसन्नता होगी कि आज तो हम बच गये ! परन्तु इसमें अपना उद्योग न मानकर भगवान्की कृपा माननी चाहिये कि
भगवान्की कृपासे आज हम बच गये, नहीं तो इसके वशीभूत हो जाते ! इस तरह साधकको कभी
भी कोई दोष दीखे तो वह उसके वशीभूत न हो और उसको अपनेमें भी न माने ।
मूल दोष है–मिली हुई स्वतन्त्रताका
दुरुपयोग । हम असत्की
सत्ता मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते; छल, कपट, हिंसा आदि कर भी सकते हैं और
नहीं भी कर सकते–यह मिली हुई स्वतन्त्रता है । जबसे हमने
इस स्वतन्त्रताका दुरुपयोग किया, तभीसे जन्म-मरण आरम्भ हुआ । इसलिये साधकको चाहिये
कि वह मिली हुई स्वतन्त्रताका दुरुपयोग न करे । दुरुपयोग न करनेसे निर्दोषता
सुरक्षित रहेगी ।
जब मिली हुई
स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करके असत्का संग करता है, तब वह असत्के संगसे होनेवाले
संयोगजन्य सुखमें आसक्त हो जाता है । संयोगजन्य सुखकी
आसक्तिसे ही सम्पूर्ण दोष पैदा होते हैं ।
(शेष आगेके ब्लॉगमें)
–‘सहज
साधना’ पुस्तकसे
|
FOLLOW BY EMAIL
कीर्तन
Labels
- आहार-शुद्धि (13)
- कर्म-रहस्य (21)
- कल्याण-पथ (13)
- गीता-दर्पण (12)
- जीवनका कर्तव्य (2)
- जीवनोपयोगी कल्याण-मार्ग (14)
- दुर्गतिसे बचो (18)
- निर्वाणदिन (1)
- भगवन्नाम (27)
- मानवमात्रके कल्याणके लिये (71)
- सत्संगका प्रसाद (27)
- साधक-संजीवनी-0-नम्र निवेदन (3)
- साधक-संजीवनी-0-प्राक्कथन (4)
- साधक-संजीवनी-अध्याय-०१ (21)
- साधक-संजीवनी-अध्याय-०२ (67)
- साधक-संजीवनी-अध्याय-०३ (59)
- साधक-संजीवनी-अध्याय-०४ (49)
- साधक-संजीवनी-अध्याय-०५ (12)
Blog Archive
-
►
2023
(313)
- November (9)
- October (31)
- September (30)
- August (31)
- July (31)
- June (30)
- May (31)
- April (30)
- March (31)
- February (28)
- January (31)
-
►
2022
(366)
- December (31)
- November (30)
- October (31)
- September (30)
- August (32)
- July (31)
- June (30)
- May (31)
- April (30)
- March (31)
- February (28)
- January (31)
-
►
2021
(364)
- December (31)
- November (30)
- October (31)
- September (30)
- August (31)
- July (31)
- June (30)
- May (31)
- April (30)
- March (31)
- February (28)
- January (30)
-
►
2020
(366)
- December (31)
- November (30)
- October (31)
- September (30)
- August (31)
- July (31)
- June (30)
- May (31)
- April (30)
- March (31)
- February (29)
- January (31)
-
►
2019
(365)
- December (31)
- November (30)
- October (31)
- September (30)
- August (31)
- July (31)
- June (30)
- May (31)
- April (30)
- March (31)
- February (28)
- January (31)
-
►
2018
(363)
- December (31)
- November (30)
- October (30)
- September (30)
- August (31)
- July (31)
- June (30)
- May (31)
- April (30)
- March (30)
- February (28)
- January (31)
-
▼
2017
(333)
- December (27)
- November (28)
- October (31)
- September (30)
- August (31)
- July (33)
- June (3)
- May (29)
- April (30)
- March (31)
- February (29)
- January (31)
-
►
2016
(367)
- December (31)
- November (30)
- October (31)
- September (30)
- August (31)
- July (31)
- June (30)
- May (31)
- April (31)
- March (31)
- February (29)
- January (31)
-
►
2015
(368)
- December (31)
- November (30)
- October (32)
- September (30)
- August (31)
- July (31)
- June (32)
- May (31)
- April (30)
- March (31)
- February (28)
- January (31)
-
►
2014
(367)
- December (32)
- November (30)
- October (31)
- September (30)
- August (31)
- July (32)
- June (30)
- May (31)
- April (30)
- March (31)
- February (28)
- January (31)
-
►
2013
(369)
- December (31)
- November (31)
- October (31)
- September (30)
- August (31)
- July (33)
- June (30)
- May (31)
- April (30)
- March (31)
- February (29)
- January (31)
-
►
2012
(385)
- December (36)
- November (34)
- October (31)
- September (31)
- August (34)
- July (32)
- June (31)
- May (31)
- April (30)
- March (34)
- February (30)
- January (31)
मेरे स्वामीजी
स्वामीजीका जन्म वि.सं.१९६० (ई.स.१९०४) में राजस्थानके नागौर जिलेके छोटेसे गाँवमें हुआ था और उनकी माताजीने ४ वर्षकी अवस्थामें ही उनको सन्तोंकी शरणमें दे दिया था, आपने सदा परिव्राजक रूपमें सदा गाँव-गाँव, शहरोंमें भ्रमण करते हुए गीताजीका ज्ञान जन-जन तक पहुँचाया और साधु-समाजके लिए एक आदर्श स्थापित किया कि साधु-जीवन कैसे त्यागमय, अपरिग्रही, अनिकेत और जल-कमलवत् होना चाहिए और सदा एक-एक क्षणका सदुपयोग करके लोगोंको अपनेमें न लगाकर सदा भगवान्में लगाकर; कोई आश्रम, शिष्य न बनाकर और सदा अमानी रहकर, दूसरोकों मान देकर; द्रव्य-संग्रह, व्यक्तिपूजासे सदा कोसों दूर रहकर अपने चित्रकी कोई पूजा न करवाकर लोग भगवान्में लगें ऐसा आदर्श स्थापित कर गंगातट, स्वर्गाश्रम, हृषिकेशमें आषाढ़ कृष्ण द्वादशी वि.सं.२०६२ (दि. ३.७.२००५) ब्राह्ममुहूर्तमें भगवद्-धाम पधारें । सन्त कभी अपनेको शरीर मानते ही नहीं, शरीर सदा मृत्युमें रहता है और मैं सदा अमरत्वमें रहता हूँ‒यह उनका अनुभव होता है । वे सदा अपने कल्याणकारी प्रवचन द्वारा सदा हमारे साथ हैं । सन्तोंका जीवन उनके विचार ही होते हैं ।
हे नाथ ! मेरे नाथ !! मैं आपको भूलूँ नहीं !
−श्रद्धेय श्रीस्वामीजी महाराज