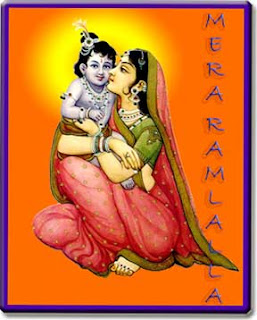भगवान् से अपनापन-६
भगवान् से अपनापन-६
(गत् ब्लॉगसे आगेका)
आप दान-पुण्य करके, बड़ा उपकार करके इतना लाभ नहीं ले सकते, जितना लाभ भगवान् के शरण होनेसे ले सकते हैं । कारण कि परमात्माके साथ हमारा अकाट्य-अटूट सम्बन्ध है । यह सम्बन्ध कभी भी टूट नहीं सकता । इस सम्बन्धको जीव ही भुला है, भगवान् नहीं भूले । इसलिये जीवके ऊपर ही भगवान् की तरफ चलनेकी जिम्मेवारी है । भगवान् तो अपनी ओरसे कृपा कर ही रहे हैं, चाहे वह कैसा ही क्यों न हो । भगवान् सबका पालन, भरण-पोषण करते हैं । पापीको दण्ड देकर सुधारते हैं, नरकोंमें डालकर पवित्र करते हैं । इस तरह भगवान् तो सम्पूर्ण जीवोंका पालन-पोषण करनेमें, उनको पवित्र करनेमें लगे हुए हैं । भगवान् कहते हैं—
सनमुख होई जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥
(मानस, सुन्दर.४४/२)
जीव ही भगवान् से विमुख हुआ है, इसलिये इस पर ही भगवान् के सम्मुख होनेकी जिम्मेवारी है । जहाँ सम्मुख हुआ कि बेडा पार ! इसलिये हम प्रभुके चरणोंकी शरण हो जायँ और अपनी अहंता बदल दें कि हम परमात्माके हैं । जैसे बहनें-माताएँ अपनी अहंता बदल देती है कि मैं अब इस घरकी नहीं हूँ; जहाँ विवाह हुआ है, उस घरकी हूँ । उनका गोत्र बदल जाता है, पिताका गोत्र नहीं रहता । कई जगह ऐसी बात आती है कि घरमें कोई बालक पैदा हुआ और सूतक लगनेके कारण हम ठाकुरजीकी सेवा नहीं कर सकते, तो कहते है कि तुम्हारी जो विवाहित लडकी घरपर है, वह सेवा कर देगी; क्योंकि उसको तुम्हारा सूतक नहीं लगता, उसका गोत्र दूसरा है । वही लडकी आपके घरमें है और उसके ससुरालमें बालक पैदा हुआ तो आप उसको कहते हैं कि देख बेटी, जलको हाथ मत लगाना । वह खास अपनी बेटी है, पर ससुरालमें बालक पैदा होनेसे सूतक लगता है । ऐसे ही आप अपनी अहंता बदल दें कि हम तो भगवान् के हैं तो आप वास्तविकतातक पहुँच जायँगे ।
हम अपनी तरफसे भगवान् को अपना मानते नहीं पर भगवान् अपनी तरफसे हमें अपना मानते हैं । मानते ही नहीं, जानते भी हैं । बच्चा माँको अपनी माँ मानता है, पर कभी-कभी अड़ जाता है कि तू मेरा कहना नहीं मानती तो मैं तेरा बेटा नहीं बनूँगा । माँ हँसती है; क्योंकि वह जानती है कि बेटा तो मेरा ही है । बच्चा समझता है कि माँको मेरी गरज है, बेटा बनना माँको निहाल करना है, इसलिये कहता है कि तेरा बेटा नहीं बनूँगा, तेरी गोदमें नहीं आऊँगा । परन्तु बेटा नहीं बननेसे हानि किसकी होगी ? माँका क्या बिगड़ जायगा ? माँ तो बच्चेके बिना वर्षोसे जीती रही है, पर बच्चेका निर्वाह माँके बिना कठीन हो जायगा । बच्चा उलटे माँपर अहसान करता है । ऐसे ही हम भी भगवान् पर अहसान कर सकते है !
भगवान् के एक बड़े प्यारे भक्त थे, नाम याद नहीं है । वे रात-दिन भगवद्भजनमें तल्लीन रहते थे । किसीने उनके लिये एक लंबी टोपी बनायी । उस टोपीको पहनकर वे मस्त होकर कीर्तन कर रहे थे । कीर्तन करते-करते वे प्रेममें इतने मग्न हो गये कि भगवान् स्वयं आकर उनके पास बैठ गये और बोले कि भगतजी ! आज तो आपने बड़ी ऊँची टोपी लगायी ! वे बोले कि किसीके बापकी थोड़े ही है, मेरी है । भगवान् ने कहा कि मिजाज करते हो ? तो बोले कि माँगकर थोड़े ही लाए हैं मिजाज ? भगवान् पूछा कि मेरेको जानते हो ? वे बोले कि अच्छी तरहसे जानता हूँ । भगवान् बोले कि यह टोपी बिक्री करते हो क्या ? वे बोले कि तुम्हारे पास देनेको है ही क्या जो आये हो खरीदनेके लिये ? त्रिलोकी ही तो है तुम्हारे पास, और देनेको क्या है ? भगवान् बोले कि इतना मिजाज ! तो वे बोले कि किसीका उधार लाये हैं क्या ? भगवान् ने कहा कि देखो, मैं दुनियासे कह दूँगा कि ये भगत-वगत कुछ नहीं हैं तो दुनिया तुम्हारेको मानेगी नहीं । वे बोले कि अच्छा, आप भी कहा दो, हम भी कह देंगे कि भगवान् कुछ नहीं हैं । आपकी प्रसिद्धि तो हमलोगोंने की है, नहीं तो आपको कौन जानता है ? भगवान् ने हार मान ली !
माँके हृदयमें जितना प्रेम होता है उतना प्रेम बच्चोंके हृदयमें नहीं होता । ऐसे ही भगवान् के हृदयमें अपार स्नेह है । अपने स्नेहको, प्रेमको वे रोक नहीं सकते और हार जाते हैं ! ‘और सबसों गये जीत, भगतसे हार्यो’ कितनी विलक्षण बात है ! ऐसे भगवान् के हो जाओ । दूसरोंके साथ हमारा सम्बन्ध केवल उनकी सेवा करनेके लिये है । उनको अपना नहीं मानना है । अपना केवल भगवान् को मानना है । भगवान् की भी सेवा करनी है, पर उनसे लेना कुछ नहीं है ।
आपकी कन्या अपनी अहंता बदल देती है, अपनेको दूसरे घरकी बहू मान लेती है । क्या आपमें उस कन्या-जितनी सामर्थ्य भी नहीं है ? जिस कन्याका आपने पालन-पोषण किया, बड़ी धूमधामसे विवाह किया, उस कन्याके बदलनेपर (दूसरे घरको अपना माननेपर) भी आप नाराज नहीं होते । ऐसे ही आप अपनेको भगवान् का और भगवान् को अपना मान लें तो कोई नाराज नहीं होगा; क्योंकि यह सच्ची बात है । मीराबाईने कहा—‘मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई ।’ गिरधर गोपालके सिवाय मेरा कोई नहीं है और मैं किसीकी नहीं हूँ ।
आप नौकरी करो तो आपकी योग्यताके अनुसार आपको तनख्वाह मिलेगी । परन्तु आप घरमें माँके पास जाओ तो क्या माँ आपकी योग्यताके अनुसार रोटी देगी । आप काम करो तो भी रोटी देगी और काम न करो तो भी रोटी देगी । इस तरह भजन करनेसे ही भगवान् से सम्बन्ध होगा, भजन न करनेसे सम्बन्ध नहीं होगा—यह बात नहीं है । यदि आप भगवान् से अपनापन कर लेंगे कि हे नाथ ! मैं तो आपका ही बालक हूँ, तो भगवान् सोचेंगे कि यह जैसा भी है, अपना ही बालक है ! अतः भगवान् को आपका पालन करना ही पड़ेगा । इसलिये ‘मैं तो आपका ही हूँ और आप ही मेरे हैं’—यह बड़ा सीधा रास्ता है ।
भगवान् कहते हैं कि यह जीव है तो मेरा ही अंश, पर प्रकृतिमें स्थित शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धिको खींचता है, उनको अपना मानता है (गीता १५/७) ! अरे किस धंधेमें लग गया ! है कहाँका और कहाँ लग गया ! संसारकी सेवा करो । अपने तन, मन, धन, बुद्धि, योग्यता, अधिकार आदिसे दूसरोंको सुख पहुँचाओ, पर उनको अपना मत मानो । यह अपनापन टिकेगा नहीं । केवल सेवा करनेके लिये ही वे अपने हैं । संसारकी जिन चीजोंमें अपनापन कर लेते हैं, वे ही हमें पराधीन बनाती हैं । वहम होता है कि इतना परिवार मेरा, इतना धन मेरा, पर वास्तवमें ये तेरे नहीं हैं, तू इनका हो गया, इनके पराधीन हो गया ! न तो ये हमारे साथ रहेंगे और न हम इनके साथ रहेंगे । इसलिये बड़े उत्साह और तत्परतासे इनकी सेवा करो तो दुनिया भी राजी हो जाय और भगवान् भी राजी हो जायँ ! आप भी सदा आनन्दमें, मौजमें रहें ! जब सेवा करनेवाला नहीं मिलता, तब सेवा चाहनेवाला दुःखी रहता है । परन्तु सेवा करनेवाला सदा सुखी रहता है, आनन्दमें रहता है ।
—‘साधन-सुधा-सिन्धु’ पुस्तकसे (पूरे लेखको पढ़नेके लिए लिंक पर क्लिक करें)
http://www.swamiramsukhdasji.org/swamijibooks/pustak/pustak1/html/sadhansudhasindhu/bhakti/bhakti8_260.htm